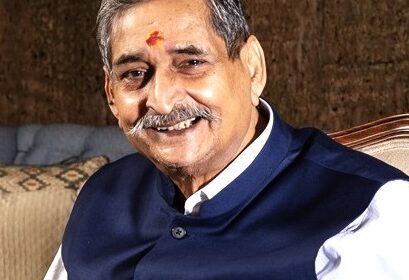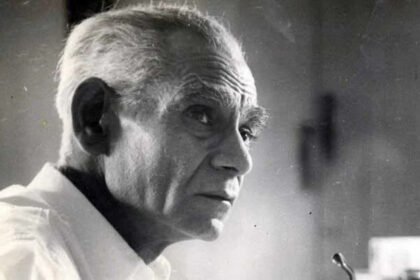नीरज कुमार दुबे (वरिष्ठ स्तंभकार)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जटिल कूटनीतिक और राजनीतिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए शुल्क बढ़ाने और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी को मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक संदेश भी है कि पश्चिम के सामने झुकने का युग अब समाप्त हो चुका है।
देखा जाये तो मोदी सरकार वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि बनकर उभरी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और नैतिक उपदेशों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने हितों को स्वतंत्र रूप से साधने की नीति अपनाई। यह वही “रणनीतिक स्वायत्तता” है, जिसकी बात भारत दशकों से करता आया है, पर जिसे आज व्यवहार में लाने का साहस शायद पहली बार किसी सरकार ने इस हद तक दिखाया है।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनौती केवल बाहरी नहीं है। देश के भीतर कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निकटता पर तंज कस रहे हैं। “माई फ्रेंड डोनाल्ड” जैसे वाक्य अब राजनीतिक व्यंग्य बन चुके हैं। कांग्रेस यह सवाल उठा रही है कि अगर अमेरिका से घनिष्ठता इतनी ही प्रभावशाली थी, तो भारत को टैरिफ धमकी क्यों झेलनी पड़ रही है? देखा जाये तो यह आलोचना राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है, पर इसमें कूटनीतिक यथार्थ की गहराई को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत आज आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से एक उभरती शक्ति है और ऐसे में विश्व के साथ उसकी मोल-भाव करने की शैली भी बदली है। मोदी जिस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह न केवल अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि विकल्पों का निर्माण भी कर रहा है— जैसे ब्रिक्स + का मंच, ऊर्जा विविधता की दिशा में कदम और नए व्यापारिक सहयोग।
इसके अलावा, ‘मोदी है तो मुमकिन है’ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इस समय एक परीक्षण की कसौटी बन चुका है। प्रधानमंत्री को अब यह साबित करना है कि वह पश्चिम के दबाव को संतुलित करते हुए, रूस से रिश्ते बनाए रखते हुए और विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता के रूप में उभार सकते हैं। देखा जाये तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोदी को तीन स्तरों पर निर्णायक पहल करनी होगी- 1. अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखते हुए, ट्रेड वार को टालना होगा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की स्पष्ट पैरवी करनी होगी। 2. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि आयात और शुल्क जैसे हथियारों का असर सीमित हो और ऊर्जा आपूर्ति में विविधता भी लानी होगी। 3. आंतरिक एकता और विपक्ष के प्रहारों का उत्तर तथ्यों और नीतिगत पारदर्शिता से देना होगा, ताकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि दिखाई दे।
देखा जाये तो यह वह घड़ी है जब प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व के अपने सबसे कठिन अध्याय में प्रवेश करना पड़ा है। लेकिन यदि वे इस दौर को सफलता से पार कर जाते हैं, तो यह केवल उनकी नहीं, बल्कि एक नए भारत की विजय होगी— जो दबाव में नहीं झुकता, हितों की रक्षा करता है और दुनिया को सम्मान के साथ संवाद करना सिखाता है। और तब शायद ‘मोदी है तो मुमकिन है’ सिर्फ चुनावी नारा नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ भी बन जाएगा।
जहां तक ताजा घटनाक्रमों की बात है तो आपको बता दें कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को सख्ती से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किये गए वक्तव्य में साफ तौर पर कहा गया है कि रूस से आयात ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता को बनाये रखने के लिए उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने यह भी उजागर किया है कि अमेरिका और यूरोप स्वयं अभी भी रूस से उर्वरक, खनिज, रसायन, यूरेनियम और एलएनजी जैसी सामग्रियों का भारी व्यापार कर रहे हैं। भारत का यह तर्क एकदम सही है कि जब तक अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त नहीं करते, तब तक भारत को नैतिकता के कठघरे में खड़ा करना न केवल दोहरा मापदंड है, बल्कि ‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’ भी।
दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर शुल्क बढ़ाने और रूसी तेल की खरीद पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी को विशेषज्ञ अमेरिका की घरेलू राजनीति और आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊँचे दामों में बेचकर लाभ कमा रहा है, साथ ही यूक्रेन युद्ध में नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा। किंतु यह आरोप राजनीतिक बयानबाज़ी अधिक लगता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पुनः बिक्री और रिफाइनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे कई देश अपनाते हैं। देखा जाये तो ट्रंप द्वारा शुल्क बढ़ाने की घोषणा एक तरफ भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को प्रभावित करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर इसे अमेरिका के कृषि और डेयरी उद्योग के समर्थन में लॉबिंग के रूप में भी देखा जा सकता है।
वहीं, रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की ‘नव-उपनिवेशवादी’ नीति का उदाहरण बताया है। क्रेमलिन का यह दावा कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ पर आर्थिक दबाव बना रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि रूस अमेरिका की एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। भारत जिस रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता आया है, उसका असली परीक्षण ऐसे ही समय में होता है जब उसे पश्चिमी दबावों, वैश्विक व्यापारिक हितों और घरेलू राजनीतिक आलोचनाओं के बीच संतुलन साधना हो। अमेरिका और यूरोपीय देशों को समझना होगा कि रूस से तेल खरीद केवल व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि भारत की एक आत्मनिर्भर और व्यावहारिक विदेश नीति का प्रतीक भी है।
पश्चिम के आगे झुकने का युग समाप्त