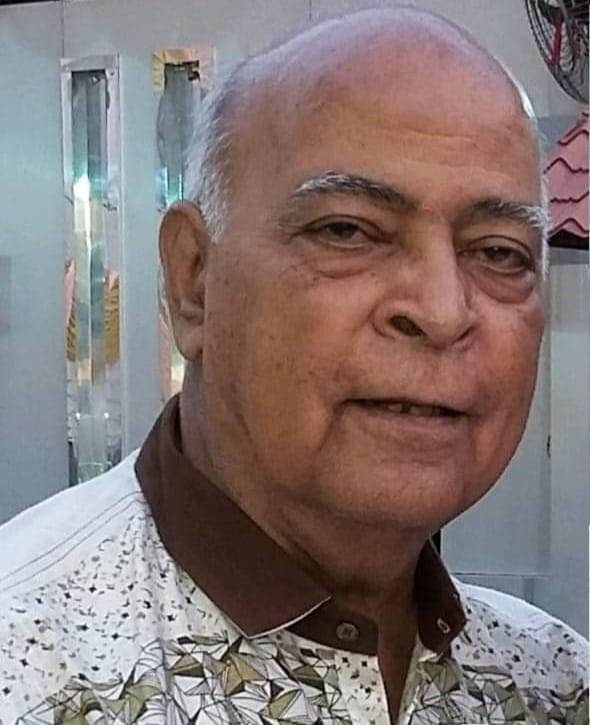अशोक भाटिया
(वरिष्ठ स्तंभकार)
द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा के गुण कूटनीतिक जटिलताओं को दिखाते हैं। भारत और चीन इसके पर्याय हैं। एशिया की दो महान शक्तियां एक दूसरे की पड़ोसी हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद ऐसी लक्ष्मण रेखा है जो राजनीतिक संबंध को सामान्य होने नहीं देती। इसका असर रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के हितों को स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। भारत और चीन दोनों विशाल बाजार हैं। चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत चीनी कंपनियों के लिए निवेश और उपभोक्ता बाजार उपलब्ध कराता है। चीन की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता तथा भारत की श्रमशक्ति और बाजार मिल कर विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं। दोनों देशों को तेल, गैस और खनिजों की भारी जरूरत है। सहयोग से आपूर्ति शृंखला मजबूत की जा सकती है।
सौर और हरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग कर भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। तीसरी दुनिया की मूलभूत समस्याएं और विकसित देशों से मिलती चुनौतियों के खिलाफ भी दोनों देश मिल कर खड़े नजर आते हैं। दुनिया भर में चीन ने अपना आर्थिक कारोबार बढ़ाया है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपना व्यापक प्रभाव कायम कर रहा है। यह स्थिति अमेरिका और यूरोप को परेशान करती है, तो भारत के लिए भी सब कुछ सामान्य नहीं है।
व्यापार असंतुलन बड़ा मुद्दा है। भारत निवेश और तकनीक चाहता है, वहीं चीन भारत के बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। एक ओर दोनों देश उभरती हुई एशियाई शक्तियां हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थक हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय नेतृत्व, सुरक्षा और वैश्विक संस्थानों में प्रतिनिधित्व को लेकर प्रतिस्पर्धा है। भारत दक्षिण एशिया में अपना पारंपरिक नेतृत्व बनाए रखना चाहता है, जबकि चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव में निवेश कर भारत के प्रभाव को चुनौती देता है। इस बीच अमेरिका द्वारा छेड़े गए टैरिफ वार ने भारत और चीन दोनों को निकट ला दिया है। दोनों देश अमेरिका की नई टैरिफ नीति का मुकाबला करने के लिए पुराणी कटुता को भूल अपने संबंध सुधरने में लग गए हैं।
दोनों देश लद्दाख के संघर्षग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रों में शुद्ध गश्त पर सहमत हुए हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के सबूत के रूप में सीमा पार व्यापार और धार्मिक पर्यटन की संभावना की ओर इशारा किया है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर भारत के साथ मतभेदों के कारण दोनों देशों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका यह भी मानना है कि व्यापार आतंक के युग में, सहयोग, सुलह और समन्वय से बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। उन्होंने अगले महीने बीजिंग में शंघाई सहयोग सम्मेलन का निमंत्रण सौंपा। मोदी ने इसे स्वीकार कर लिया।
भारत छोड़ने के बाद वह अफगानिस्तान गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। उस चर्चा के केंद्र में अफगानिस्तान से चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना का विस्तार करना था। चीन भारत के साथ सहयोग की बात करता है और वह भी चीन। भारत ने अफगानिस्तान को अभी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है लेकिन चीन ने वहां परियोजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए 80 फीसदी हथियार चीन निर्मित थे। चीन निकट भविष्य में देश को नवीनतम लड़ाकू जेट प्रदान करके देश को और अधिक युद्ध के लिए तैयार करने का इरादा रखता है।
एक तरफ चीन रणनीतिक तरीके से भारत पर हमला करना चाहता है, दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर यह हमारे लिए अपरिहार्य होता जा रहा है। यदि वह दुर्लभ यौगिकों की आपूर्ति को नियंत्रित करना चाहता है, तो हमारा ऑटो विनिर्माण क्षेत्र घुसपैठ कर रहा है। हम अक्सर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में खुद की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक कच्चे माल का मुख्य स्रोत चीन है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, अधिकांश घटक और उप-घटक चीन से आते हैं। दूसरे शब्दों में, 2020 के बाद, हमारे नाजुक पड़ोसी को बाहर निकालने के लिए राजनयिक और सैन्य प्रतिरोध के साथ-साथ आर्थिक प्रतिबंधों के हथियार का उपयोग करने की मजबूत मांग थी।
पांच साल बाद, भारत-चीन व्यापार में देश का हिस्सा 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वहां हमारा निर्यात अभी भी खंडित है, लेकिन वहां से माल का आयात साल दर साल बढ़ रहा है। इस असंतुलन से एक और खतरा संभव है। हमें यह समझना होगा कि हमसे ज्यादा मजबूत होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों में चीन की भाषा क्यों बदल गई है। उन्होंने इसे पर्याप्त जोखिम नहीं दिया। इसलिए उनके लिए इसे कम करने और फिर जबरन शुल्क लगाने के बाद भी इसे थोड़ी देर के लिए निलंबित करने का समय आ गया था।
लेकिन ट्रम्प पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ताकि अगर वार्ता रुक जाए और अमेरिका सख्त टैरिफ लगाए, तो एक बड़ा बाजार चीन के लिए शत्रुतापूर्ण हो सकता है। ऐसी स्थिति में, चीन को अज़रा बाजार खोजना होगा जो चीन के निरंतर उत्पादन चक्र के लिए चीन की भूख को संतुष्ट करता है। भारत इन मानदंडों पर उच्च स्थान पर है। यह मुख्य कारणों में से एक है कि चीन ने ब्रिक्स समूह को क्यों रखा है। भारत, ब्राजील, आदि। अब इंडोनेशिया चीनी सामानों के लिए एक ‘ड्रेनिंग ग्राउंड’ हो सकता है, यही वजह है कि ट्रम्प ने इसे मान्यता दी है, यही वजह है कि वह लगातार ब्रिक्स को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को इस खतरे को पहचानना चाहिए।
चीन की शत्रुता व्यक्त और प्रत्यक्ष है, लेकिन मैत्री वार्ता के पीछे की दुश्मनी ज्ञात और अनकही है। यह बार-बार प्रदर्शित किया गया है कि नेहरू के नेतृत्व वाले भारत ने इसे मान्यता नहीं दी। चीन उन विद्वान शासकों तक पहुंचने में भी विफल रहा है जिन्होंने बार-बार कहा है कि उन्होंने इसे मान्यता नहीं दी है। हम कई वर्षों से विनिर्माण, बुनियादी ढांचे के निर्माण, खनन, रोजगार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महाशक्ति रहे हैं । लेकिन इसने मध्यम शक्तियों के अनुरूप प्रगति भी नहीं की है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से सेवा-उन्मुख, कृषि-केंद्रित, उपभोक्ता-केंद्रित है। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में, आवाज और वजन केवल उत्पाद-उन्मुख और निर्यात-उन्मुख देशों के लिए हैं। जब तक यह स्थिति नहीं बदलती, हमारे विकल्प सीमित हैं। यह काफी स्पष्ट है कि यह रहेगा।
प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। इस यात्रा का महत्त्व सीमा पर स्थिरता बहाल करने, व्यापार, उड्डयन, कूटनीति में सुधार और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने जैसे कई आयामों से जुड़ा है। यह केवल एक बहुपक्षीय सम्मेलन में उपस्थिति भर नहीं है, बल्कि भारत-चीन संबंधों, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने वाला कदम हो सकता है। भारत को चीन के साथ संघर्ष और सहयोग दोनों का संतुलन साधना पड़ेगा।
भारत के सामने यह जटिल चुनौती है कि वह अमेरिका और यूरोप से अत्याधुनिक तकनीक, पूंजी और बाजार का लाभ उठाए, रूस के साथ पारंपरिक रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखे और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद सीमित सहयोग की संभावनाएं खुली छोड़े। यह बहुआयामी संतुलन भारत को बना कर रखना होगा। किसी संप्रभु राष्ट्र के लिए शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाएं महत्त्वपूर्ण है और राष्ट्र की सुरक्षा उसका दायित्व है। अमेरिका की नीतियां और चीन से मजबूत संबंध स्थापित करने की कोशिशें भारत की विदेश नीति के लिए परीक्षा की घड़ी है।
भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियां कितनी सार्थक