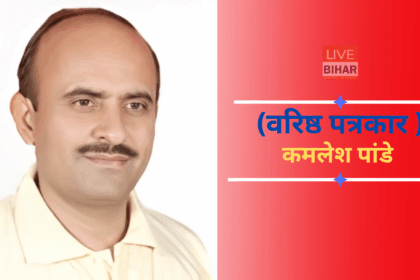डॉ. कुलवीर सिंह चौहान (प्राध्यापक )
परतंत्र और स्वतंत्र भारत की राजनीति को सम्यक दिशा देकर भाषायी एवं क्षेत्रीय अस्मिताओं के दायरे से बाहर निकालकर देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अछुण्य रखने में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान था। 6 जुलाई 1901 को सर आशुतोष मुखर्जी व योगमाया देवी के सुयोग्य पुत्र के रुप में कोलकाता में जन्मे डॉ. मुखर्जी में सनातन धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं, वैज्ञानिक एवं अकादमिक अभिरुचियों के प्रति गहरा लगाव था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मात्र 23 वर्ष की अवस्था में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट के फैलो बनाए गए थे। 1934-38 के अवधि में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा (33 वर्ष की अवस्था) और सफल कुलपति होने का गौरव भी उन्होंने प्राप्त किया।
यह बंगाल ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी देश के विश्वविद्यालयी इतिहास में सबसे युवा कुलपति बनने का एक कीर्तिमान भी था। इसके पहले 1929 व 1937 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1939 में विनायक दामोदर सावरकर की प्रेरणा से हिन्दू महासभा में शामिल हुए तथा 1941 से 1947 तक हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हिन्दूओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया।1946 में वह संविधान सभा के सदस्य बने।1947 से 1950 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तथा हिन्दू हितों की अनदेखी के कारण नेहरू-लियाक़त समझौते के विरोध में मंत्रिमंडल से 8 अप्रैल 1950 को त्यागपत्र दे दिया और 21 अक्टूबर,1951 को अखिल भारतीय स्वरुप के ‘भारतीय जनसंघ, नामक दल का गठन किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विभाजनकारी नीतियों और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उभार से जो जहर भारतीय शासन व्यवस्था में व्याप्त हो रहा था, डॉ. मुखर्जी ने उनसे निपटने का वैचारिक एवं क्रियात्मक दोनों स्तरों पर प्रयास किया। डॉ. मुखर्जी पिछड़े वर्गों के आधार पर संरक्षण के अतिरिक्त धार्मिक आधार पर किसी भी विशेष संरक्षण या भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। वह विभाजन की शर्तों पर स्वाधीनता प्राप्ति के मुखर विरोधी थे।
20वीं शताब्दी का आरम्भ भारत की राजनीति का वह दौर था जिसमें राजनीतिक पराधीनता के साथ वैचारिक अंतर्विरोध और सांस्कृतिक संकट के लक्षण परिलक्षित हो रहे थे। सारे देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक तीव्र लहर चल रही थी। भारत द्वितीय विश्वयुद्ध में श्रीहीन व शक्तिहीन हो चुके ब्रिटिश शासनतंत्र की बेड़िया तोड़ने को तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज इस स्थित को भांप कर भारत से विदा लेने के पहले बड़े षड्यंत्र को रच रहे थे। इसी साजिश के तहत अंग्रेजों ने बंगाल, जो भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना का मुख्य केंद्र रहा था,के विभाजन की कुटिल चाल चली। परंतु इस विद्वेषपूर्ण ब्रिटिश नीति ने राष्ट्रवाद की धारा को मंद करने के स्थान पर और तीव्र कर दिया था। स्वाधीनता संघर्ष की परिणति भारत की आजादी थी, किंतु विभाजन की त्रासदी ने देश को गहरी वेदना दी। विभाजन की अनिवार्यता को भांप कर, डॉ. मुखर्जी ने बंगाल, असम व पंजाब के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान के चंगुल में जाने से बचा लिया। डॉ. मुखर्जी के दूरदर्शी प्रयासों से ही सगर-पुत्रों की तपोभूमि, बंकिमचन्द्र, सुभाषचंद्र बोस, विवेकानंद, कवीन्द्र-रवींद्र,बंदा बैरागी,गुरुगोविंद सिंह की पावन धरा पश्चिम बंगाल व पंजाब का पाकिस्तान में विलय होने से बचाया जा सका।
स्वाधीन भारत के पहले मंत्रिमंडल में 15 अगस्त 1947 को वह महात्मा गाँधी के आग्रह और स्वातंत्र्यवीर सावरकर की प्रेरणा से शामिल हुए। यह भी अपने आप में एक रोचक तथ्य है कि कांग्रेस की नीतियों के धुर विरोधी दो विद्वान राजनेताओं डॉ. मुखर्जी व डॉ. अम्बेडकर को उनके नेतृत्व क्षमता, वक्तता कौशल व दूरदर्शी दृष्टिकोण के चलते नेहरु मंत्रिमंडल में उद्योग व आपूर्ति तथा कानून व श्रम जैसे अति महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। इस विश्वास को कायम रखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर लगातर किए जा रहे अत्याचारों व देश में भीषण दंगो के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरु द्वारा पाक प्रधानमंत्री लिकायत अली को भारत में मुस्लिम समस्याओं के संदर्भ में भेजे आमंत्रण प्रस्ताव से खिन्न होकर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। 16 जनवरी 1951 को आयोजित एक बैठक में पार्टी के घोषणापत्र व संविधान पर चर्चा के बाद भारतीय जनसंघ नामक एक राष्ट्रीय दल के गठन का निर्णय हुआ। 21 अक्टूबर,1951 को जिस दिन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, दिल्ली में चार सौ प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इस नवीन संगठन के अध्यक्ष के रुप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संस्थापक अध्यक्ष घोषित किया गया।
कानपुर में जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय की मांग का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि ‘एक देश में दो प्रधान,दो विधान व दो निशान-नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे’। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने दलीय एकाधिकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने जनसंघ के प्रथम अधिवेशन कानपुर में उड़ीसा के राजनीतिक दल गणतंत्र परिषद् को अधिवेशन में आमंत्रित किया था।प्रथम आम चुनाव में सारे देश से जनसंघ के मात्र 3 सांसद व कुल 17 विधायक (9 बंगाल व 8 राजस्थान से) पार्टी के टिकट पर चुने जा सके। जनसंघ एक नवजात राजनीतिक दल था।इसके बावजूद जनसंघ के घोषणापत्र में चुनाव पूर्व घोषित जमींदारी उन्मूलन की नीति का राजस्थान के जागीरदार विधायकों के विरोध को उन्होंने ठीक न मानते हुए 6 विधायकों को उनके जमींदारी उन्मूलन के जनसंघ के समर्थन का विरोध करने के कारण डॉ. मुखर्जी के निर्देश पर जनसंघ से निष्कासित किया गया था। इससे प्रकट होता है कि सामाजिक न्याय व दलीय अनुशासन के प्रति वह कितने समर्पित राजनेता थे!
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर उन्होंने आंदोलन किया ही, किन्तु हैदराबाद और जूनागढ़ राज्यों के भारतीय संघ में विलय की बाधाओं को दूर कराने में भी डॉ. मुखर्जी ने सरदार पटेल के साथ मिलकर मंत्रिमण्डलीय बैठकों के निर्णयों को राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में मोड़ने का सफल प्रयास किया। डॉ. साहब इस बात से बहुत व्यथित थे कि देश के नागरिकों को अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए अनुमति-पत्र/परमिट लेनी पड़ती है। इसीलिए जब देश के दो प्रमुख सांसदों उमाशंकर त्रिवेदी तथा विष्णु घनश्याम देशपाण्डे को बिना परमिट के प्रवेश की अनुमति न देकर गिरफ्तार कर लिया गया तो डॉ. मुखर्जी ने इसे देश के नागरिकों का स्वदेश में अपमान मानते हुए प्रजा परिषद् द्वारा किए जा आंदोलन को समर्थन देने व राज्य में प्रवेश की परमिट व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से 8 मई को जम्मू-कश्मीर की ओर प्रस्थान किया। 23 जून 1953 को श्रीनगर के एक बंगले में नजरबन्दी के रुप में रहस्यमय परिस्थियों में उनकी मौत ने सारे देश को स्तब्ध कर दिया।
हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु, उर्वरक कारखाना, सिंदरी तथा लोकोमोटिव कारखाना, चित्तरंजन, इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन, आल इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड, आल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे संस्थान डॉ. मुखर्जी की औद्योगिक नीति (1948) की देन है। स्वावलंबन व स्वदेशी के मार्ग पर चलकर इस नीति में उन्होंने वस्त्र उद्योग के व्यापक विस्तार की योजना को मूर्त रूप दिया। उसी का यह प्रतिफल है की भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में आज वस्त्र उद्योग की सबसे बड़े उद्योगों में गिनती होती है। भिलाई और राउरकेला में कालांतर में स्थापित इस्पात संयंत्रो की पृष्ठभूमि भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मंत्रित्व काल में ही बनी। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यूनिवर्सिटीज कालेज आफ साइंस व शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय, कोलकाता जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानो के प्रशासनिक समितियों में रहकर उन्होंने इन संस्थानों की संवृद्धि के भरसक प्रयास किए। 1943 में बंगाल में आए भीषण अकाल के समय पीड़ितो के लिए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर को लिखे गए मार्मिक पत्रों व सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में सक्रिय भूमिका के लिए उन्हे आज भी याद किया जाता है। डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता के साथ कभी समझौता नहीं किया।
भारतीय भाषाओं के संपोषण का प्रश्न रहा हो अथवा मातृभाषा बांग्ला के प्रति आदर व अनुराग का भाव।वह पूर्ण रुप से भारत व भारतीयता के प्रति समर्पित थे।स्नातक में अंग्रेजी में उत्कृष्ट अंक अर्जित करने बावजूद अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी की सलाह पर उन्होंने बांग्ला भाषा में एम.ए.किया और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। डॉ. मुखर्जी द्वारा विज्ञान की शिक्षा बांग्ला में उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली का संकलन कराया गया।कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉ. मुखर्जी की पहल पर 1937 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में प्रथम दीक्षांत भाषण हुआ। चाहे हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने की मुहिम रही हो या उर्दू, हिन्दी और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं के बी.ए. पाठ्यक्रमों को कलकत्ता विश्वविद्यालय में आरम्भ करवाने का निर्णय, डॉ. मुखर्जी ने औपनिवेशिक भाषातंत्र के स्थान पर भारतीय भाषाओं की संवृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।
वे मानते थे कि प्रत्येक देश को अपनी मातृभाषा में शिक्षा एवं न्याय उपलब्ध होना चाहिए। डॉ. मुखर्जी देश भारत की भाषाई एकता के लिए हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच संयोजन के पक्षधर थे। वह पाश्चात्य शिक्षा के दुष्प्रभावों से परिचित हो चुके थे अतः उनका मानना था कि समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना भारतीय भाषाओं की एकात्मता से ही हो सकती है। डॉ. मुखर्जी का भाषाई अनुराग इतना गहरा था कि 1926 में इंग्लैंड में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने बांग्ला समेत सभी भारतीय भाषाओं के एकीकरण का पुरजोर समर्थन किया था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में उनकी आस्था नहीं थी। डॉ. मुखर्जी व जनसंघ दोनों का विचार था कि भाषाई संरक्षण देश की संस्कृति को मजबूत करने में सहायक होगा। वह भारत में ही नहीं विश्व की शिक्षण संस्थाओं मातृभाषाओं के संरक्षण के हिमायती थे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में ‘बहुभाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन’ डॉ. मुखर्जी के भारतीय भाषानुराग को ही प्रतिबिंबित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वयन के वर्तमान भाषायी गतिरोध का समाधान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश की भाषा समस्या पर उनके विचारों के क्रियान्वयन से किया जा सकता है। डॉ.मुखर्जी पर साम्प्रदायिक, रुढिवादी, कट्टर हिन्दू आदि होने के आरोप लगाएं जाते हैं, जो सही नही है। बंगाली साहित्यकार नजरुल इस्लाम को उनके द्वारा की गयी आर्थिक व चिकित्सकीय सहायता रही हो, उर्दू भाषा के संवर्धन के उनके प्रयास रहें हो अथवा महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते बुद्ध के अवशेषों के संदर्भ में की गयी उनकी यात्राएं। वस्तुतः वह सर्वधर्म समभाव व वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय परंपरा के संवाहक थे। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का अब तक एकांगी विश्लेषण ही हुआ है।
उम्मीद है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक व अकादमिक अवदान का व्यापक नजरिए से मूल्यांकन होगा तथा उनके वैचारिक उत्तराधिकारी के रुप में सत्तारूढ संप्रति केन्द्र सरकार डॉ. साहब के शैक्षिक, राजनीतिक वैज्ञानिक योगदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक अभियान को आगे बढाएगी। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करने, वक्फ संशोधन कानून एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारत केंद्रित शिक्षा के क्रियान्वयन के संकल्प से राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिला है। आशा है कि देश में विश्वविद्यालयों सहित स्कूली शिक्षा संस्थानों को परीक्षा लेने की संस्थाओं के स्थान पर शिक्षा दीक्षा, शोध व अनुसंधान के गुरुकुलों में बदलने, विकास में स्वदेशी साधनों संसाधनों पर निर्भरता, कृषक कल्याण व भारतीय संस्कृति के संरक्षण के ठोस प्रयासों सहित अन्य राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी निर्भीक व संकल्पबद्ध निर्णय होंगे। जिससे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को सही मायनों में साकार किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय एकीकरण के नायक: डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी