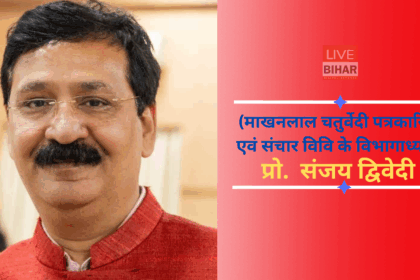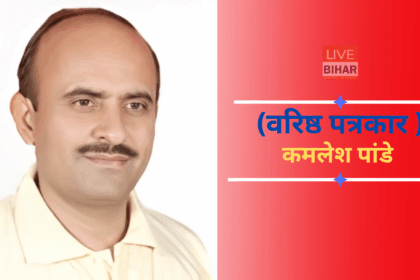प्रेमकुमार मणि
सवाल कुछ अटपटा है. लेकिन यह सवाल मेरे मन में कभी- कभार उठता है. मैं नहीं जानता औरों के मन में उठता है या नहीं, या उठता है तो वे इस पर किस तरह सोचते हैं. प्रेमचंद ( 1880-1936 ) उन्नीसवीं-बीसवीं सदी के लेखक हैं. पांच साल बाद उनकी 150 वीं जयंती मनाई जाएगी. 1980 में जब उनकी सौवीं जयंती दिल्ली के फिक्की सभागार में धूमधाम से मनाई गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने किया था, मैं शामिल हुआ था. वह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, जिसमें दुनिया भर के लेखक इकठ्ठा हुए थे. तब मैं युवा था और मुझे थोड़ा-सा इस बात का गुमान हुआ था कि मैं उस जुबान में लिखता हूँ जिसके लेखक प्रेमचंद हैँ. रवीन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद आधुनिक भारतीय साहित्य के ऐसे दो सितारे हुए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली. वह हमारी राष्ट्रीय पहचान हैं. हिन्दी के तो हैं ही.
मैं कोई प्रेमचंद विशेषज्ञ नहीं हूँ , लेकिन कह सकता हूँ कि उनकी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. मानसरोवर के सभी खंड कॉलेज के दिनों में ही पढ़ गया था. लगभग सभी उपन्यास भी. उनकी एक छोटी-सी किताब है ‘ रामचर्चा ‘ ; उसे भी पढ़ गया हूँ. उनके बहुत सारे अग्रलेख जो उनकी पत्रिकाओं में छपते थे , वह भी पढ़ा हूँ. मुझे उनकी कई कहानियां बेहद पसंद है. बड़े से बड़े लेखक का सब कुछ अच्छा ही नहीं होता. रोटी-पानी केलिए भी लेखक को लिखना पड़ता है. मानसरोवर की बहुत-सी कहानियां केवल गिनती के लिए हैं. लेकिन यह भी है कि प्रेमचंद के यहाँ कम से कम बीस ऐसी कहानियां हैं, जिनमें उनका युग धड़कता है. उनके माध्यम से उनके ज़माने को समझा जा सकता है. ऐसे ही उनके उपन्यासों में गबन, निर्मला, रंगभूमि और गोदान ऐसे हैं जिन से उन्हें और उनके जमाने को समझा जा सकता है.
प्रेमचंद का जीवन-काल केवल छप्पन वर्षों का है. यह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन अथवा भारत में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का भी सघन दौर है. उनका जन्म 1880 में होता है. इसके पांच साल बाद कांग्रेस का जन्म होता है. जब वह पचीस की उम्र में थे तब बंग-भंग आंदोलन शुरू हुआ और इसके साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन सगुन दौर में आ गया. इसी बीच मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठन बने और कुछ साल बाद राष्ट्रीय क्षितिज पर गांधी का उभार हुआ. कांग्रेस, हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग आम-जन के संगठन नहीं थे. ये जमींदार और कुलीन हिन्दू-मुस्लिम अवाम के संगठन थे,जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय से अधिक वर्गीय था. 1857 में इसी तबके ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था. इनका संघर्ष केवल इसलिए था कि अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम लोग यानी हिन्दू-मुस्लिम कुलीन जन, जिनका यकीन रजवाड़ी ढाँचे में था, यहाँ राजसत्ता पर काबिज हों. जनता के नाम पर इनके साथ दकियानूसी लोग थे, जो बाद में भी मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा के सहयोगी बने.
कांग्रेस भी वैचारिक स्तर पर दो भागों में बँटी हुई थी. एक तबका दकियानूसी था, तो दूसरा सुधारवादी. दकियानूसी तबके का नेतृत्व तिलक कर रहे थे और सुधारवादियों का गोखले. 1907 के सूरत कांग्रेस में कोहराम और जूतम-पैजार के बाद तिलक को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया. लेकिन सुधारवादी कुछ अधिक अंग्रेजपरस्त हो गए. सुधारवादियों के नेता गोखले की तत्कालीन वायसराय से एक वार्ता चर्चा में थी कि जब वायसराय ने उनसे पूछा कि मिस्टर गोखले यदि अंग्रेज भारत छोड़ने का निर्णय लें तो आप क्या करेंगे? गोखले का जवाब था हम स्वागत करेंगे, लेकिन जब आप लंदन पहुंचेंगे तब तक हमारा टेलीग्राम आपको मिलेगा कि आप कृपया लौट आवें. उपरोक्त हाल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का था. गांधी आए तो उन्होंने खिलाफत का समर्थन कर कुलीन मुस्लिम तुष्टिकरण का ऐसा पाशा फेंका कि उसकी भीषण सामाजिक प्रतिक्रिया हुई. हिन्दू और मुसलमानों में सामाजिक दकियानूसीपन को ताकत मिली और राष्ट्रीय आंदोलन दिग्भ्रमित हुआ.
प्रेमचंद यह सब देख-समझ रहे थे. ऐसे समय में जब असहयोग आंदोलन के विफल हो जाने से राष्ट्रीय नैराश्य फैला हुआ था, 1924 में उनकी कहानी आती है ‘ शतरंज के खिलाड़ी ‘. यह कहानी पूरी तरह राजनीतिक है. इसमें वर्णित अवध को आप पूरा हिंदुस्तान मान लीजिए. वह राष्ट्रवादी इतिहासकारों के इस बकवास को सीधे नकारते हैं कि यहाँ अंग्रेज चालबाजी या छल-कपट से आए. नहीं, हम अपनी आदतों में विलासी और अपनी सोच में दकियानूसी थे, इसलिए अंग्रेज यहाँ आए. कहानी की शुरुआत ही होती है ‘ वाजिद अली शाह का समय था, अवध विलासिता के रंग में डूबा था. ‘ सामंतवाद की इस पराकाष्ठा पर सामंत भी राजनीतिक चेतना से इतने शून्य थे कि बिना एक कतरा लहू बहाए उनका बादशाह पकड़ कर ले जाया जा रहा है और शोहदे सामंत अपनी शतरंज की मोहरों केलिए मर मिटते हैं. और ऐसा क्यों करते हैं कि लड़ने भिड़ने से बच निकलने वाले लोग, जो खिलाड़ी बन कर रह गए हैं, अपने मोहरे केलिए मर मिटते हैं. प्रेमचंद की टिपण्णी उसी कहानी में है ‘ उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था. ‘ किसी हिंदुस्तानी इतिहासकार ने इस गुत्थी को नहीं समझा था. बाल्ज़ाक को समझने केलिए कार्ल मार्क्स थे, प्रेमचंद को समझने केलिए यहाँ कोई नहीं था.
प्रेमचंद का वास्तविक लेखन काल 1920 से 1936 है. इसके पूर्व उन्होंने जो लिखा वह उनकी तैयारी थी. इन सोलह वर्षों में उन्होंने दहेज़ पर बलि चढ़ी निर्मला को देखा, गहनों के प्रति भारतीय स्त्रियों के लगाव पर चोट करता उनका उपन्यास ‘गबन’. फिर अछूत समस्या को लेकर लिखी गयी कहानी ‘ ठाकुर का कुआँ’ और पुरोहितवाद को सीधी चुनौती देती हुई उनकी कहानी ‘ सद्गति’ और ‘ सवा सेर गेहूं. ‘ ये सब राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक शक्ति प्रदान कर रही थीं. केवल अंग्रेज अंग्रेज मत करो, अपनी कमजोरियों को देखो. तुमने अपनी ही जनता के बड़े हिस्से को गुलाम बना कर रखा है, तुम्हें अपनी आजादी की लडाई लडने से पहले अपने सामंती-पुरोहितवादी चरित्र को त्यागना होगा. आजादी का मतलब व्यापक होता है. किसानों, स्त्रियों, दलित समूहों को गुलाम रख कर तुम अपनी आजादी सुरक्षित नहीं रख सकते.
1930 के बाद उन्होंने एक कदम और बढ़ाया. उन्हें साहित्य में एक प्रतिमान भी गढ़ना था. कफ़न, पूस की रात जैसी कहानियां और गोदान जैसा उपन्यास इसी प्रक्रिया में लिखे गए. 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था. प्रेमचंद काफी व्यस्त थे. उन्हें पत्रकारिता भी करनी थी, लेखन भी करना था, सभा-सम्मेलनों में जगह-जगह जाना भी इसी बीच अधिक हुआ. उनके विचार उनके अग्रलेखों में आये. वह समाजवादी विचार और नेहरू के व्यक्तित्व के सम्मोहन में दीखते हैं. उनकी चिन्ता है कि किस तरह उत्तरभारतीय समाज का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तरक्कीपसंद बने. वह दकियानूसी तत्वों से जूझते हुए साहित्य में लगभग अकेले दीखते हैं. उन्हें कोई नहीं समझ सका. उनके पाठक उनकी लोकप्रियता को ही रेखांकित करते हैं, उनके विचारों को दरकिनार कर दिया जाता है.
मैं प्रेमचंद के गाँव लमही में कोई पचीस साल पहले गया था. मुख्य सड़क से थोड़ी दूर हट कर उनका गाँव था. उनका घर एक किनारे पर ही था, जिसके बगल में बांस की छोटी-सी बाड़ी थी. घर अपने समय के ख्याल से बहुत अच्छा रहा होगा. दोमंजिला पक्का घर. हालांकि मैं जब गया था तब वह जीर्ण-शीर्ण हो चुका था. पलस्तर टूटे थे और किंवाड़ें सड़ कर टूट-बिखर गई थीं. कुछ किताबें नजर आईं, लेकिन सड़ी-गली स्थिति में. उन्हें छूना स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक हो सकता था. इन सब के बीच मेरा ध्यान उस पक्के कुँए, जिसका आधा हिस्सा घर के भीतर और आधा हिस्सा घर के बाहर था, पर रहा. गाँव के लोगों ने बताया प्रेमचंद जी ने कुँए के आधे हिस्से को सार्वजनिक किया हुआ था. उनके कुँए से दलित भी पानी निकाल सकते थे. दलितों ने जब कुँए का इस्तेमाल किया तब गाँव के सवर्णों ने कुँए का वहिष्कार किया. यह जानकारी मेरे लिए खास थी.
दूसरी खास चीज थी कोई नब्बे साल के एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात जो बांस बाड़ी के निकट एक टूटी खाट पर लेटे हुए थे. जानकारी मिली ये प्रेमचंद जी के सेवक रहे थे. बिरादरी के हिसाब से दलित चमार. वह प्रेमचंद को बाबा कह रहे थे. इन दो जानकारियों ने मुझे बताया कि प्रेमचंद अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे थे. वह 1936 में मरे. तब पूना पैक्ट हो गया था और गांधी ने अपना हरिजन आंदोलन शुरू कर दिया था. प्रेमचंद कोई दलित नेता नहीं थे. पूना पैक्ट के समय अनेक लोगों को दलित समस्या का एहसास उस तरह नहीं था जिस तरह आम्बेडकर को था. गांधी भी बहुत बाद जाकर इस समस्या पर गंभीर हुए. उन्होंने इसे राष्ट्रीय नजरिये से देखा. प्रेमचंद भी इसी रूप में देख रहे थे. उनका राष्ट्रवाद किसानों, स्त्रियों और उत्पीड़ित समूहों विशेष कर दलितों के ताने बाने से बना था. अपने निजी जीवन में भी उन्होंने इन मूल्यों को शामिल किया हुआ था.
मेरा सवाल फिर मेरे कन्धों पर सवार है. प्रेमचंद आज होते तो क्या करते ? मेरे जहन में एक ही विचार आता है. निश्चित ही वह पुरस्कारों केलिए अछूत घोषित कर दिए गए होते. कोई संस्था या सरकार उन्हें कोई पुरस्कार देने की हिम्मत नहीं करती. लिटफेस्ट जैसे आयोजनों से वह बाहर होते. आज वह किसानों, मजदूरों, उत्पीड़ित समूहों की मुक्ति और लोकतान्त्रिक मूल्यों केलिए लगातार लिख रहे होते. बहुत संभव है उन्हें अर्बन नक्सली घोषित कर किसी जेल में ठूंस दिया गया होता और हर जन्मदिन के रोज हम उनके जेल जीवन के साल गिन रहे होते.
प्रेमचंद यदि आज होते….