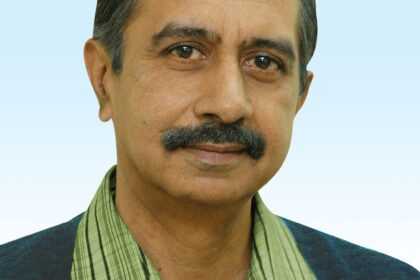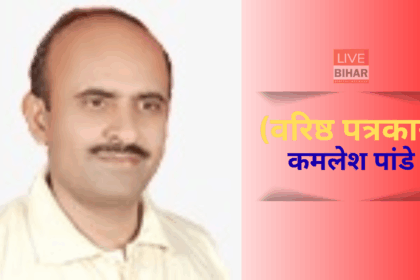प्रेम कुमार मणि (साहित्यकार )
कुछ लोग मानते हैं कि लेखक का लिखा हुआ देखना चाहिए, उसके व्यक्ति रूप से उसे जोड़ कर नहीं देखना चाहिए. यानि रचना की स्वतंत्र तौर पर विवेचना होनी चाहिए. उसके रचनाकार के व्यक्तित्व से उसकी रचना का एकात्म होना आवश्यक नहीं है. एक ख़राब व्यक्ति भी अच्छा लेखक हो सकता है. इस उलझन में मैं भी लम्बे अरसे तक रहा. अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा तभी संभव है जब हम रचना को ईश्वरीय कृति मान लें. जैसे वेद,कुरान आदि ईश्वरीय कृति है, वैसे ही तमाम साहित्य ईश्वरीय कृति है और लेखक की भूमिका एक स्टेनोग्राफर भर की है.
मैं मानता रहा हूँ कि रचना और रचनाकार के बीच एक अयुत संबंध होता है. दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे जगत और चेतना; एक दूसरे से सापेक्ष हैं, एक दूसरे पर अवलम्बित. इसीलिए उन्नीसवीं सदी के रूसी आलोचक-चिन्तक निकोलाय चेर्नीशेव्स्की ( 1828 1889 ) की इस बात से मैं सहमत हूँ कि रचना का मूल्यांकन करने के पहले रचनाकार को देखो. मैं इस में रचना-काल यानी उस दौर को भी देखे जाने का हिमायती हूँ. यानि रचनाकार की भौतिकता उसके कर्म अथवा उत्पाद को प्रभावित करती है. वैदिक ऋषियों और उपनिषद के रचनाकारों का समय और जीवन अलग-अलग था. इसका प्रभाव दीखता है. वेदों का देवता इंद्र है. खाने पीने वाला लम्पट तबियत का व्यक्ति. जाने कितने गौतमों के घरों में घुसा और कितनी अहिल्याओं का शीलहरण किया. दरअसल वैदिक ऋषियों के चरित्र में ही छोटे छोटे इंद्र पल रहे थे. इसके भौतिक आधार थे. वैदिक ऋषि अपनी आर्थिक संरचना में सर्वहारा थे. उपनिषदों के रचयिता राजन्य थे. उनके घर के कोठार अन्न से भरे थे. पेट भरा था. उन्होंने ब्रह्म का सृजन किया, जो खाता पीता नहीं है. भरे पेट का आदमी उपवास कर उल्लास हासिल करता है और भूखा आदमी खूब खा पी कर.
यह केवल भारत की बात नहीं, दुनिया भर में होता रहा है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य एशिया के धार्मिक ग्रन्थ कुरान की मीमांसा कम हुई है, लेकिन यदि उसकी मीमांसा करें तो दिलचस्प नतीजे आएंगे. कुरान के आरंभिक और आखिरी हिस्से में एक गहरा तनाव दीखता है. यह मुहम्मद की उम्र और उनकी भौतिक स्थितियों में आये परिवर्तन का भी परिचय देता है. इसलिए मैं इस मत का हूँ कि लेखक को उसकी रचना या उसे उलट कर कहें तो रचना को लेखक से जोड़ कर ही देखा जाना चाहिए. तुलसी और कबीर या खुसरो और जायसी की रचनाओं को देखिए. उनके जीवन को देखे बिना उनकी रचनाओं का मूल्यांकन अधूरा होगा. मुझे हमेशा अनुभव होता रहा है कि रामचरित मानस तुलसी की आत्मकथा है और मेघदूत कालिदास की आत्मव्यथा. इसे अलगा कर देखना सही नहीं होगा. कबीर की कविता में तुलसी की कविता के मुकाबले उल्लास अधिक है तो इसका कारण यह है कि तुलसी के जीवन में कबीर के मुकाबले अधिक दारिद्र्य और हाहाकार था. कबीर चदरिया बुनते थे, उनकी आमदनी तय थी; वह तुलसी की तरह भीख पर पेट नहीं पालते थे.
लेकिन यह सब तो लेखक और उसकी रचना का अंतर्संबंध हुआ. चर्चा लेखक की नैतिकता की करना चाहता था. क्या लेखक की नैतिकता का कोई अर्थ है या नहीं? क्या लेखक को आवारा, सर्वतंत्रस्वच्छंद और गैर जिम्मेदार होना चाहिए या उसे संत, ऋषि महर्षि व्यक्तित्व का होना चाहिए? क्या लेखक और आमजन की नैतिकता में भेद भी संभव है?
मैं समझता हूँ किसी दौर का लेखक चरित्रहीन न हुआ है, न हो सकता है. उसमें एक किस्म का आवारापन हो सकता है ,जो उसकी स्वच्छंदता का द्योतक है, उसकी अराजकता का नहीं. उसके शब्दानुशासन में उसका चरित्रानुशासन प्रतिबिंबित होता है. पुराने ज़माने के जिन ऋषि लेखकों की हम बातें करते हैं वह अपने समय के हिसाब से विचारों की दुनिया बना रहे थे. उनकी दुनिया आज की लोकतान्त्रिक दुनिया नहीं थी. उनकी दुनिया आज की तरह मनुष्य केंद्रित नहीं, देवता केंद्रित थी. उनका मानना था कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह अधिक से अधिक देव केंद्रित हो जाय. एक लम्बे संघर्ष के बाद मनुष्य जाति ने दुनिया को मनुष्य केंद्रित किया. और आज हमारा सारा ध्यान मनुष्य की गरिमा स्थापित करने की है. दुनिया को मनुष्य केंद्रित करने केलिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा. आज भी वह संघर्ष चल रहा है. जो ऋषियों का दायित्व था, उसे लेखकों ने अपनी व्याख्या के साथ अपने जिम्मे ले लिया. पुरानी दुनिया के चौकीदारों ने इन लेखकों का प्रतिकार किया. रूसो, वाल्तेयर जैसे लेखक विचारकों ने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली हैं, उसे देखना चाहिए. आज के लेखक की नैतिकता तुलसी और कबीर जैसी नहीं है. वे माला नहीं जपेंगे, नारे लगाएंगे. उन्हें देवताओं की दुनिया नहीं, मनुष्यों की दुनिया गढ़नी है. उन्हें मंदिर मस्जिद नहीं, संसद गढ़ने हैं. उनकी मंजिल कठिन है, चुनौती कड़ी है,इसलिए उनकी नैतिकता भी अधिक पुख्ता होगी. यदि यह नहीं है, तो लेखक अपने ज़माने की चुनौतियों का सामना करने में अक्षम होगा. वह कलमघिस्सू बन कर रह जाएगा. जैसा कि हमारी हिंदी के ज्यादातर लेखक हैं. क्या किसी को लगता है कि लेखक को ऐसा होना चाहिए ?
आज के लेखक की नैतिकता का अर्थ यह नहीं कि वह ब्रह्मचारी, शाकाहारी और सुरापान से तौबा करने वाला हो. उसकी नैतिकता का अर्थ यह है कि वह अपने सत्य पर किस सीमा तक अड़ा रहने वाला है. वह अपने सत्य का मोलभाव तो नहीं कर रहा ? जिस मुकम्मल आज़ादी की प्रस्तावना वह अपनी कविताओं, कहानियों या दूसरी विधाओं में करता है, क्या वह उन्हें अपने जीवन में उतारता है क्या. अपने प्रेम की स्वच्छन्तता का परचम उठाने वाला लेखक कवि क्या अपनी पत्नी, प्रेमिका या पुत्री के जीवन में उनके ऐसे ही व्यवहार का समर्थन करने से भागता तो नहीं है. यदि वह भागता है तो वह अनैतिक है. फ्रांसीसी लेखक ज्यां जेने चोरी करते थे और समलैंगिग भी थे. लेकिन उन्होंने इसे छुपाया नहीं. सार्त्रे ने उन पर किताब लिखी है और उन्हें संत जेने बताया है. लेखक का सत्य आम आदमी के सत्य से इसी अर्थ में अलग है कि उसमें संतत्व के दर्शन होते हैं.
आज का साहित्य अपने चरित्र में सेकुलर है. सेकुलर का अर्थ हिन्दू मुस्लिम एकता नहीं, इनकी अवहेलना. जैसा कि पहले ही कहा वह मनुष्य केंद्रित है. कोई धर्मग्रन्थ, पुरोहित, ईश्वर उसके लक्ष्य में नहीं है, उसका लक्ष्य मनुष्य है. उसकी गरिमा और आज़ादी है. इसलिए आज के लेखक को अधिक जिम्मेदार अधिक नैतिक होना है. उसे अपने छोटे से छोटे व्यवहार पर नजर रखनी है. मुझे स्मरण होता है 1980 के दशक का ब ब कारंत और विभा मिश्र काण्ड. नाट्यकर्मी विभा मिश्र आग से बुरी तरह झुलस गयी थीं. कारंत साहब पर आरोप लगे. उनकी गिरफ्तारी हुई. उनके शिष्यों की संख्या बड़ी थी. लोग जुटे. कारंत साहब से कहा गया कि वह झूठ बोल दें कि वहां नहीं थे. उन्होंने झूठ बोलने से इंकार किया. उन्होंने सहवास तक को कबूला और कहा कि आग मैंने नहीं, उसने खुद लगाईं. मैं बचाव करने में थोड़ा झुलसा. विभा जब अस्पताल में होश में आईं तब उन्होंने भी कहा कि नहीं कारंत साहब का इस में कोई दोष नहीं था. यह एक रचनाकार की नैतिकता होती है. कारंत एक कलाकार थे. वह अपने सत्य पर अड़े रहे. विभा नहीं बचतीं तो उन्हें फांसी हो सकती थी. लेकिन कारंत अपने सत्य पर रहे.
मिर्ज़ा ग़ालिब यदि शराब पीते थे तो छुपाते नहीं थे. मस्जिद में भी बैठ कर पीने का दम रखते थे. जन्नत की हकीकत को समझते हुए भी दिल बहलाने को उसका ख्याल बनाए रखना चाहते थे. वह जुआ खेलने का शौक पालते थे और इसके जुर्म में हवालात भी गए थे. लेकिन बचने केलिए उन्होंने इंकार नहीं किया कि मैं नहीं खेलता हूँ. मीरा ने प्रेम किया तो ढोल बजा कर किया. ऐसी नैतिकता होती है लेखक की. यह वर्ष लेखक मोहन राकेश की जन्मशती का है. उनकी मृत्यु के बाद दिनमान का जो अंक आया था उसके मुखपृष्ठ पर उनका फोटो था. लेकिन भीतर के पृष्ठों पर उनके संस्मरणों में से एक था कि एक बार उपप्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुछ लेखकों को चाय पर बुलाया. राकेश भी थे. अपनी आदत से लाचार राकेश ने सिगरेट सुलगाई. गांधीवादी मोरारजी को बुरा लगा. उन्होंने आवेश में कहा राकेश जी, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता. राकेश भी वैसे ही थे. तपाक से जवाबा, बदतमीजी कौन कर रहा है, मैं या आप ? चाय पर बुला कर भाषण पिला रहे हैं. और राकेश उठ कर निकल गए.
तो इस तरह का साहस और इस तरह की नैतिकता लेखक की होती है. शराब और सिगरेट पीने, नहीं पीने, ब्रह्मचारी रहने और अहिंसक रहने न रहने से नैतिकता का कोई वास्ता नहीं है. ये आचरण निश्चित तौर से श्रेय हैं. लेकिन नैतिकता के मानदंड नहीं. आप यदि जरूरत समझते हैं तो सिगरेट या शराब लीजिए. लेकिन झूठ मत बोलिए. इसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखिए. कोई गलती भी हुई है तो इसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए. अपनी गलतियों को स्वीकार करना उसके लिए क्षमा निवेदन या प्रायश्चित करना मनुष्यता के गुण हैं. लेकिन अपने अपराध को छुपाना, उसे समर्थन में अनर्गल दलील पेश करना किए गए अपराध से भी बड़ा अपराध है. कोई लेखक यह करता है तो फिर वह लेखक नहीं रह जाता. आग में पारा साधने जैसा चरित्र और चेतना लेखक का होता है. उसकी नैतिकता ऐसी ही होनी चाहिए.
साहित्य ईश्वरीय कृति है और लेखक स्टेनोग्राफर