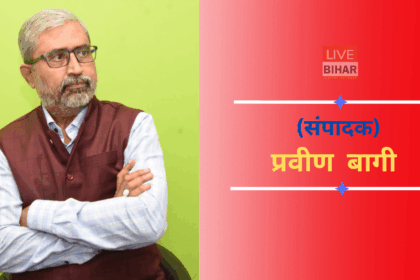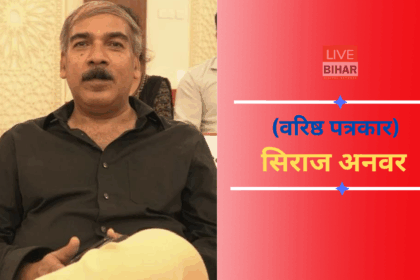गणेश दत्त पाठक (वरिष्ठ स्तंभकार)
हम जलवायु परिवर्तन की विभीषिका को अपने आस पास महसूस कर रहे हैं। इस बार उत्तरी भारत में गर्मी कम पड़ी तो दो साल पूर्व जाड़े में ठिठुरन से आम जनता बेहाल हो गई थी। पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे तथ्य मानव अस्तित्व और पारिस्थितिकी के लिए बड़े संकट बनते जा रहे हैं। डिजिटल क्रांति के दौर में ऊर्जा एक बड़ी आवश्यकता भी है। जीवाश्म ईंधनों मसलन कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद आदि ने पर्यावरण को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ऐसे में उम्मीद की किरण अक्षय ऊर्जा के संसाधन ही नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की शाश्वत विकास की अवधारणा यानी ऐसा विकास, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे, में अक्षय ऊर्जा संसाधनों मसलन सौर, पवन आदि के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आधार पर अक्षय ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहे हैं लेकिन ये प्रयास फलीभूत तभी होंगे, जब आम जन अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को समझेंगे और उसके उपयोग के लिए आगे आयेंगे। लेकिन वर्तमान में यह समझना आवश्यक है कि अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए भी जरूरी है।
मानव सभ्यता के विकास के क्रम में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ने हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को जरूर पूरा किया है लेकिन इन जीवाश्मीय ऊर्जा संसाधनों से निकले कार्बन डाई ऑक्साइड आदि हरित गृह गैसों ने धरती को गर्म किया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ने मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियों को उत्पन्न किया है। जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों की सीमित उपलब्धता ने ऊर्जा संकट की आशंका को भी उत्पन्न किया है। पर्यावरण अवनयन के दुष्प्रभावों के संदर्भ में शाश्वत विकास की संकल्पना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समन्वित ऊर्जा प्रबंधन एक अनिवार्य तथ्य है, जिसके लिए अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना भी जरूरी है।
सबसे पहले हमें अक्षय ऊर्जा स्रोत के महत्व को समझना होगा। अक्षय ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति किए जा सकते हैं तथा जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। मसलन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि। अक्षय ऊर्जा के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। प्रदूषण कम फैलता है और पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता में कमी आती है और विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है। साथ ही, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने से ऊर्जा लागत में कमी आती है, जिससे संसाधन प्रबंधन में हर स्तर पर सहायता मिलती है।
एक तथ्य यह भी है कि अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की स्थापना और रखरखाव की लागत अधिक आती है। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक शिल्प तकनीक के विकास की प्रक्रियाएं अभी चल रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की शुरुआती लागत अभी बहुत ज्यादा आ रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए निरंतर शोध और अनुसंधान एक अनिवार्य तथ्य है। आवश्यकता अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की भी है ताकि अक्षय ऊर्जा के विकास में अधिक पूंजी और विशेषज्ञता का उपयोग भी किया जा सके। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विद्युत ग्रिड में एकीकृत करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करने की आवश्यकता भी गंभीरता से महसूस की जा रही है। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के रुक रुक कर ऊर्जा उत्पादन की प्रकृति के कारण ऊर्जा भंडारण समाधानों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जागरूकता के प्रसार द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और स्वीकृति प्राप्त करना भी आवश्यक है।
भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा नीति को लागू किया गया है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और त्वरित मूल्य ह्रास लाभ प्रदान करने की व्यवस्थाओं को संजोया गया है। भारत सरकार ने री इन्वेस्ट सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया है जो अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देता है और वैश्विक निवेश धारकों को भारतीय ऊर्जा हितधारकों के साथ जोड़ता है। भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाओं को लागू किया है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों को पावर ग्रिड में एकीकृत करने में मदद करते हैं। भारत सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक असर यह हुआ है कि जनवरी 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100.33 गीगावाट हो चुकी है। भारत सरकार ने अंतराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की पहल की है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाना है। किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पी एम कुसुम योजना को संचालित किया जा रहा है।
बिहार सरकार ने भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दे दिया है। बिहार सरकार निवेश को आकर्षित करने, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयास कर रही है। अभी हाल में ही प्रत्येक घर मेंं सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही गई है जिसके अंतर्गत सब्सिडी सहयोग भी शामिल है।
निश्चित तौर पर सरकारी स्तर पर अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं विशेष तौर पर सौर ऊर्जा फॉर्मों, पवन ऊर्जा पार्कों के लिए भूमि सुरक्षित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के सार्थक प्रयास हो और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बंजर भूमि के उपयोग की व्यवस्थाओं को संजोया जाय। ग्रिड स्थिरता को बनाए रखना और रुकावटों का प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है।अक्षय ऊर्जा से संबंधित नीतियों की स्थिरता और नियामक ढांचा की व्यवस्था की स्पष्टता और उसमें सुधार की आवश्यकता को भी महसूस किया जा रहा है।
हर व्यक्ति को अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के लिए अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास करने चाहिए। इस संदर्भ में हर व्यक्ति के छोटे छोटे प्रयास अच्छी उपलब्धियों को हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मसलन सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए सब्सिडी आदि प्रदान कर रही है। इस सुविधा का लाभ उठाकर प्रत्येक व्यक्ति को सौर ऊर्जा के उपभोग के लिए आगे आना चाहिए। उद्यमियों को भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आगे आना चाहिए। प्रशासनिक मशीनरी को भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए संवेदनशील और समर्पित प्रयास करने चाहिए। सामुदायिक संगठनों को भी अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में जागरूकता के प्रसार के प्रयास करने चाहिए। इस संदर्भ में जितनी सामुदायिक भागीदारी बढ़ेगी उतनी ही सकारात्मक उपलब्धि हासिल की जा सकेगी।
आज हमारी प्रकृति एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे तथ्य हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है तो अक्षय ऊर्जा संसाधन भविष्य के लिए आशा की किरण हैं। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को समझना उसके विकास के लिए सार्थक प्रयास और सामुदायिक सहभागिता वर्तमान की आवश्यकता है तो आइए शाश्वत विकास में सहभागिता निभाने के लिए अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग का संकल्प लें।
शाश्वत विकास के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग का संकल्प लें राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विकास दिवस 20 अगस्त पर विशेष