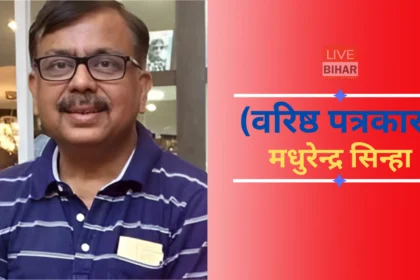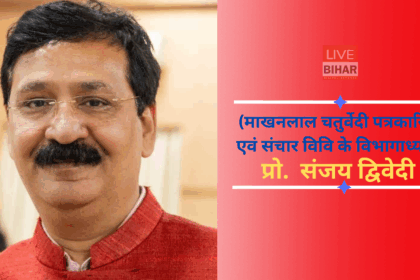राधा रमण (वरिष्ठ पत्रकार)
वैसे तो देश की राजनीति में 1957 के चुनाव में ही बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले (अब बेगुसराय जिला) के मटिहानी विधानसभा चुनाव में हो गई थी। उस समय दबंगों ने जबरदस्ती बूथ पर कब्जा कर अपने पक्ष में लोगों के वोट डलवा लिये थे। हालांकि उस काले अध्याय की चर्चा आजतक होती है। लेकिन बाद के दिनों में बूथ कैप्चरिंग की वारदातें लगातार बढ़ती गईं। राजनीति जिसकी लाठी, उसकी भैंस सरीखी हो गई। राजनीति में अपराधियों के पदार्पण की मूल वजह भी यही है। वरना आजादी के बाद की राजनीति इतनी खराब नहीं थी। सियासत के क्षेत्र में अच्छे लोग सक्रिय थे जो समाज का भला-बुरा सोचते थे। किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे कि बेटी की शादी अगर गलत घर में हो जाए तो परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन वोट अगर गलत व्यक्ति को मिल जाता है तो समाज खराब हो जाता है।
क्या आज की राजनीति और आज के समाज को आप अच्छा समाज कहना चाहेंगे ? पिछले करीब चार दशक से राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सभी दलों के नेता हो-हल्ला मचाते रहे हैं। संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी यह मसला सिर चढ़कर बोलता रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि नेता खुद भी नहीं चाहते कि राजनीति साफ-सुथरी हो। राजनीति को समाज सेवा का दर्जा दिया गया है लेकिन आजादी के बाद से हमारे समाज सेवकों की सम्पत्ति में अकूत वृद्धि हुई है। अगर, मेरी बात पर भरोसा न हो तो सरकार किसी न्यायिक आयोग से सभी नेताओं की जो किसी सदन के सदस्य रहे हों, उनकी सम्पत्ति की जांच क्यों नहीं करा लेती ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार विधायक या सांसद क्या बन गए, नेताओं की सम्पत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ जाती है।
मंत्रियों का तो कहना ही क्या ! हद तो यह कि समाज सेवा के नाम पर उन्हें टैक्स में छूट भी मिलती है। और तो और, सांसद- विधायक जब चाहते हैं अपनी तनख्वाह में मनमानी वृद्धि कर लेते हैं। आज तक इस मामले में किसी सदन में कभी विरोध की बात नहीं देखी-सुनी गई। गजब तो यह कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद् चारों सदनों का सदस्य रहा हो तो किसी सदन की सदस्यता नहीं रहने पर वह चारों सदनों के एक साथ पेंशन का हकदार हो जाता है। जबकि निजी सेक्टर में काम करनेवाले और जीवन खपाने वाले लोग बुढापे में पाई-पाई के मोहताज हो जाते हैं। आज भी लालू प्रसाद और आनन्द मोहन जैसे न जाने कितने लोग सजायाफ्ता होने के बावजूद प्रतिमाह लाखों रूपये पेंशन के ले रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि इस मामले में राजनीतिक दलों में गजब की एकता है – ‘हमाम में सभी नंगे हैं’ की उक्ति चरितार्थ होती है।
हाल ही में सजायाफ्ता सांसदों – विधायकों समेत अन्य नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने संबंधी जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया हलफनामा गौर करने लायक है। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इसपर सरकार का कहना है कि ‘याचिका में जो अनुरोध किया गया है वह संविधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से क़ानून बनाने का आदेश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से पूरी तरह परे है। इस तरह की योग्यता तय करना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।‘
सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उपयुक्त होगा या नहीं, यह पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दंड के क्रियान्वयन को एक उपयुक्त समय तक सीमित कर, रोकथाम सुनिश्चित की गई है और अनावश्यक कठोर कार्रवाई से बचा गया है। सरकार ने कहा कि यह क़ानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ‘अदालत ने निरंतर यह कहा है कि एक विकल्प या दूसरे पर विधायी विकल्प की प्रभावकारिता को लेकर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता।‘ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोषसिद्धि की तारिख से छह साल या कारावास के मामले में रिहाई की तारीख से छह साल तक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग के पास ताकत है कि वह किसी मामले में इस अवधि को कम या पूरी तरह हटा सकता है। धारा 8 कहती है कि किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह सजा पूरी करने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी तरह धारा 9 में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार अथवा देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है जिन पर से आयोग ने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया था या हटा दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि वह चुनाव आयोग से जानकारी मिलने के दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में ही यह याचिका दाखिल की थी, लेकिन सरकार की हीलाहवाली और टालमटोल रवैये के कारण मामला अभी तक परिणति तक नहीं पहुंच पाया है।
सवाल उठता है कि जो सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के उस फैसले को अध्यादेश के जरिये पलट देने की सामर्थ्य रखती हो जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहभागिता को अपरिहार्य माना गया था। उस सरकार को सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ? क्या सरकार ऐसा नहीं चाहती कि राजनीति से अपराधियों का सफाया हो अथवा सरकार में बैठे लोग कहीं अपने भविष्य को लेकर आशंकित तो नहीं हैं। नेताओं को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता यह सब देख रही है। इतिहास गवाह है कि जनता जिस तेजी से किसी को सिर पर बैठाती है जायज वजह मिलने पर उससे दूनी गति से सत्ता से च्युत भी कर देती है। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है न कि हठधर्मिता से। हमारे नेताओं को यह बात समझनी ही होगी।
राजनीति के अपराधीकरण पर कौन लगाए रोक