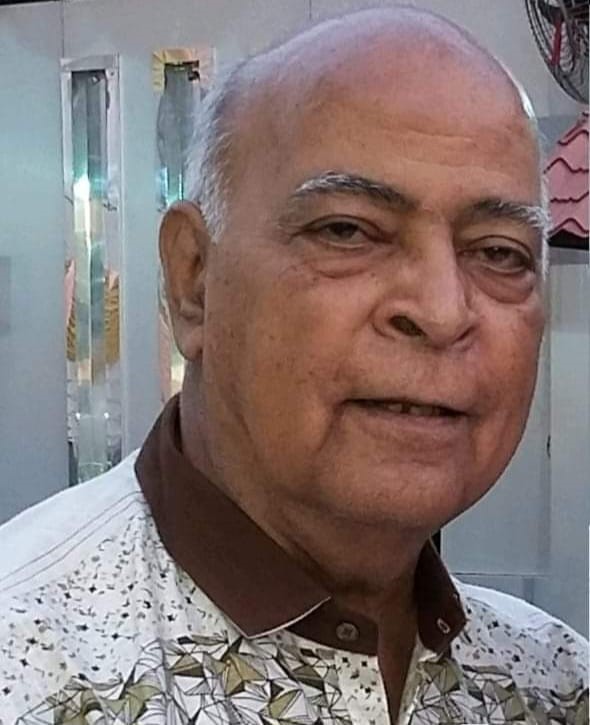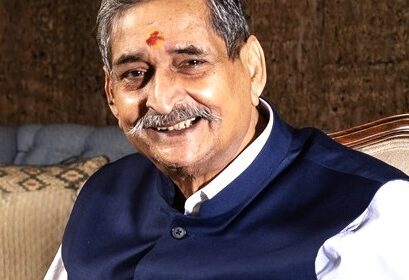उत्तरकाशी जिले में एक गांव धराली, जिससे लगा हुआ इलाका है खीरगंगा। ट्रैकिंग पर जाने वालों के लिए सबसे पसंदीदा जगह। 5 अगस्त को अचानक यहां बादल फटा। फिर पलक झपकते सारा इलाका बह गया। मकान तिनकों की तरह उखड़ गए। बाजार, बस्तियां, इंसान और मवेशी सभी बह गए। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। जिस छोटे से पहाड़ी नाले ने इस भयावह आपदा को जन्म दिया उसे स्थानीय लोग खीर गाड़ भी कहते हैं। यह 10-12 किलोमीटर ऊपर की पहाड़ियों के पन ढालों से निकलने वाली कई जलधाराओं से मिलकर बनता है। बरसात को छोड़कर साल के ज्यादातर मौसम में इसमें बहुत कम पानी रहता है। इसी के जल ग्रहण क्षेत्र में कहीं बादल फटने के कारण अचानक तेज गति के साथ बहने वाले पानी ने अपने साथ आई गाद, मिट्टी और पत्थरों के जरिए धराली को तबाह कर दिया।
खीर गाड़ या खीर गंगा जहां पर भागीरथी से मिलती है, उसी जगह पर धराली है। वहां से एक पैदल रास्ता मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा के लिए जाता था। जिस पर खीर गाड़ पार करने के लिए लकड़ी के छोटे-छोटे दो-तीन पुल बने हुए थे। बड़े छोटे पत्थरों का जमावड़ा था और उनके बीच में कहीं-कहीं बहुत छोटी-छोटी जलधाराएं दिखाई देती थी।आपदा के प्रारंभिक वीडियो में साफ दिखता है की पानी के प्रवाह में आने वाले ज्यादातर भवन इस इलाके में बने हैं जिसे प्रकृति ने अपनी चेतावनी के रूप में छोड़ा था। आपदा की चपेट में आने वाले अधिसंख्य भवन होमस्टे या स्थानीय लोगों के छोटे-छोटे होटल हैं। कुछ बड़े होटल भी आपदा की चपेट में आए हैं और आपदा का शिकार होने वाले ज्यादातर भवन नए बने हुए हैं।
बहुत तीव्र ढलान में बहने वाली खीरगाड़ का जलागम क्षेत्र बहुत अस्थिर नहीं है और वहां किसी तरह का मानवीय दखल भी नहीं है। हर की दून की तरफ जाने वाले कुछ पर्वतारोहियों और स्थानीय पशु चारकों के अलावा उस इलाके में लोगों की ज्यादा आवाजाही भी नहीं है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपदा का जन्म प्राकृतिक कारणों से हुआ है, लेकिन आपदा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव जिस इलाके में हुआ वह प्रकृति के साथ मानवीय घुसपैठ का परिणाम है।खीर गंगा के अलावा हरसिल के ऊपरी इलाकों में भी कुछ छोटी नदियों में इसी तरह की बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर यह है कि हरसिल के पास भागीरथी का प्रवाह थम सा गया है और वहां पर एक झील बनने की आशंका है।
बताया जाता है कि उत्तराखंड में बादल फटने की तबाही हर साल होती है। आखिर पहाड़ी ऊंचे इलाकों पर इतने ज्यादा बादल क्यों फटते हैं ? इससे पहले बरसात के इस मौसम में हिमाचल प्रदेश में कई बादल फटने से तबाही की खबरें आ चुकी हैं। जब बादल फटते हैं तो अचानक अथाह पानी दावानल बनकर टूट पड़ता है। इससे इतनी तेज फोर्स के साथ अचानक बाढ़ आती सब कुछ बहा ले जाती है। मकान के मकान ताश के पत्तों की तरह उड़ जाते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में एक दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, अब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में डेढ़ गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून की बारिश के दौरान ही होती हैं।
बादल फटना भारी बारिश की गतिविधि को कहते हैं। हालांकि, बहुत भारी बारिश की सभी घटनाएं बादल फटना नहीं होतीं। बादल फटने की एक बहुत ही विशिष्ट परिभाषा है। लगभग 10 किमी x 10 किमी क्षेत्र में एक घंटे में 10 सेमी या उससे अधिक बारिश को बादल फटने की घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार, उसी क्षेत्र में आधे घंटे की अवधि में 5 सेमी बारिश को भी बादल फटने की श्रेणी में रखा जाएगा।बादल फटने की घटना के दौरान, किसी स्थान पर एक घंटे के भीतर वार्षिक वर्षा का लगभग 10% वर्षा हो जाती है। औसतन, भारत में किसी भी स्थान पर एक साल में लगभग 116 सेमी वर्षा होने की उम्मीद की जा सकती है।
बादल फटना कोई असामान्य घटना नहीं है, खासकर मानसून के महीनों में। ये घटनाएं ज़्यादातर हिमालयी राज्यों में होती हैं जहां स्थानीय स्थलाकृति, विंड सिस्टम और निचले व ऊपरी वायुमंडल के बीच टेम्परेचर ग्रेडिएंट ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि, हर घटना जिसे बादल फटना कहा जाता है, वास्तव में परिभाषा के अनुसार बादल फटना नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये घटनाएँ काफी लोकल होती हैं। ये बहुत छोटे क्षेत्रों में होती हैं जहां अक्सर बारिश मापने वाले उपकरण नहीं होते।
इसके अलावा साल 2023 में जारी एक शोध पत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के शोधकर्ताओं ने बादल फटने की घटना को एक छोटी-सी अवधि में 100-250 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से अचानक होने वाली बारिश के रूप में परिभाषित किया है, जो एक वर्ग किलोमीटर के छोटे-से दायरे में दर्ज की जाती है। इस शोधपत्र को ‘इंटरनेशल हैंडबुक ऑफ डिजास्टर रिसर्च’ में प्रकाशित किया गया है।
गंगा के मायके में भागीरथी नदी का यह जल ग्रहण क्षेत्र पहले भी इस तरह की घटनाओं का गवाह रहा है। 6 अगस्त 1978 को धराली से कुछ किलोमीटर नीचे भागीरथी नदी की ही एक बहुत छोटी सहायक कनोडिया गाड़ में बादल फटने के कारण एक अस्थाई अवरोध बन गया था । जिसने टूट कर अंततः भागीरथी के जल प्रवाह को रोक दिया और बाद में 6 और 10 अगस्त को वह पूरी भागीरथी घाटी में एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में तबाही लेकर आया था।
17 जून 2013 को भी उत्तराखंड में अचानक हुई मूसलधार वर्षा 340 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी जो सामान्य 65।9 मिमी से 375 प्रतिशत ज्यादा थी। जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी दौरान अचानक उत्तरकाशी के डोडी ताल इलाके में बादल फटने के बाद असी गंगा और भागीरथी में जल स्तर बढ़ गया था। लगातार होती रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जल स्तर भी तेजी से बढ़ा। कुमाऊं हो या गढ़वाल मंडल, बारिश ने हर जगह तबाही मचाई। 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ क्षेत्र में सर्वाधिक तबाही हुई। केदारनाथ मंदिर सहित पूरी केदार घाटी में तीर्थयात्रियों सहित 5000 से अधिक लोगों की जान गई। हजारों घर, पुल, सड़कें और गांव तबाह हो गए।
इस वर्ष भी अब तक ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट-यमुनोत्री मार्ग पर बलिगढ़ में 28 जून की रात को बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई।इस प्राकृतिक आपदा के कारण एक निर्माणाधीन होटल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। घटना में 9 मजदूरों की जान चली गई। बादल फटने के कारण अचानक बढ़ गए पानी ने यमुनोत्री हाइवे को भी भारी नुकसान पहुंचाया। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण मंदाकिनी और अलकनंदा नदी घाटियों में भी बादल फटने और भूस्खलन की अनेक घटनाएं हुई हैं। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी बादल फटने से तबाही के समाचार हैं। इन घटनाओं में जनधन की भारी हानि हुई है।अनेक इलाकों में खेती की जमीन खत्म हो गई है और पशुओं को भी जान गंवानी पड़ी है।
बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं एक जटिल मुद्दा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति से छेड़छाड़ दोनों ही भूमिका निभाते हैं। इसके लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ।फ्लैश फ्लड एक ऐसी आपदा है जो अचानक आती है और भारी नुकसान करती है। मंडी जैसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और ग्लोबल वॉर्मिंग के परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासन और लोग मिलकर पहले से तैयारी करें, तो इस तरह की आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मौसम की सटीक जानकारी, बेहतर जल प्रबंधन, और पर्यावरण संरक्षण जैसे कदम हमें इस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर अपनी धरती और अपने लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें।
ये भी पढ़ें…मीडिया में यह तीसरा आदमी कौन है